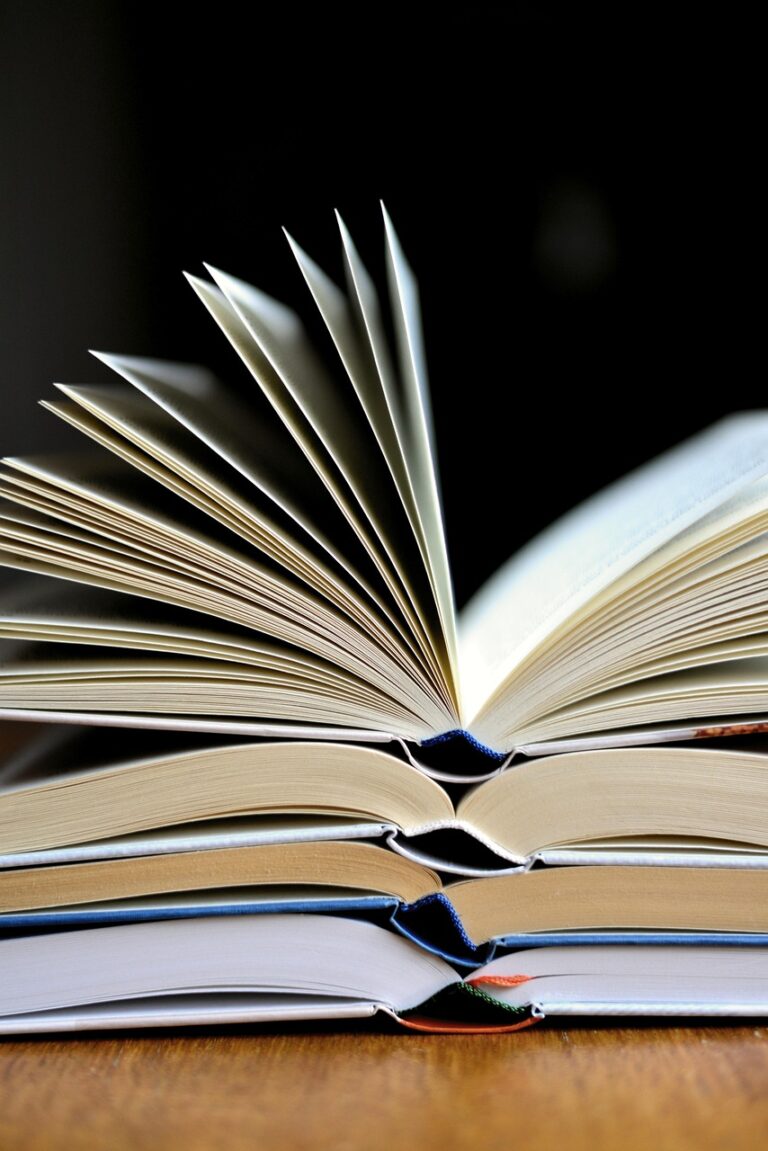भूजल का बढ़ता संकट उसके भयावह स्तर तक गिरने का अहम कारण उसका बेतहाशा दोहन है। मौजूदा दौर में भूजल स्तर में गिरावट जहां भयावह खतरे का संकेत है, वहीं पीने के साफ पानी की कमी के भीषण संकट की चेतावनी भी है। भूजल दोहन अपने चरम पर है जिसका परिणाम है कि देश के उत्तरी गांगेय इलाके में भूजल खत्म होने के कगार पर है। नतीजा यह हुआ कि पहले से ज्यादा जिले सूखे की मार झेलने को विवश हुए और शहर-दर-शहर के नल सूखने लगे।
अच्छे मानसून के अभाव के चलते अत्याधिक उपयोग से भूजल की मांग बढ़ने से जहां उसकी गुणवत्ता खराब हुयी, वहीं उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थों और भारी धातुओं की मौजूदगी ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता चला गया। यही नहीं भूजल में कमी के चलते पृथ्वी की धुरी 4.36 सेमी की दर से खिसक रही है जो खतरनाक संकेत है। इसके बावजूद हमने जल की मंहगी परियोजनाओं को प्रमुखता दी और मांग सापेक्ष दृष्टि रखने और जल के मितव्ययता के साथ उपयोग तथा भूजल रिचार्ज की कोई नीति बनाने पर कभी ध्यान ही नहीं दिया।
जमीन का वह हिस्सा जहां पानी इकट्ठा होता है, जिसे एक्यूफायर कहते हैं, से जैसे-जैसे पानी खत्म होता जायेगा,वैसे वैसे ही वहां की जमीन सिकुड़कर बैठती चली जायेगी और वहां जमीन का धंसना शुरू हो जायेगा।
पानी के मामले में हमारा देश दुनिया का सबसे समृद्ध देश है लेकिन इसके बावजूद जल संकट की गंभीरता बेहद चिंतनीय है। देश में 1960 के बाद से पानी की मांग दोगुना से भी ज्यादा हो गयी है।हालात सबूत हैं कि आज ज्यादातर स्मार्ट सिटी का पानी पीने लायक नहीं है और हिमालयी शहर सहित देश के बड़े शहर, गांव-कस्बे तक पानी के संकट से जूझ रहे हैं। अमृत सरोवरों से कुछ आस बंधी थी लेकिन आजतक एक भी अमृत सरोवर के निर्माण पूरा न होने से वह आस भी टूट चुकी है। ऐसी स्थिति में कैसे सहेजेंगे बारिश के पानी की बूंद? उस स्थिति में जबकि नीति आयोग 2030 तक घटते भूजल स्तर के कारण बड़े खतरे की चेतावनी दे चुका है।
भारत में संभावित भूजल भंडार 432 लाख हैक्टेयर है और दोहन योग्य सकल भूजल की मात्रा 396 लाख हैक्टर मीटर है। बारिश के दिनों में हर साल यह पुनर्जीवित होता है। अतः भूजल का दोहन उसकी प्राकृतिक भूमिका तथा अवांछित घटकों के सुरक्षित निष्पादन को समझकर करना बेहद जरूरी है जो उसका निरापद प्रबंधन है। लेकिन दुख है कि हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिस पर गर्व किया जा सके। नीति आयोग की मानें तो देश की साठ फीसदी आबादी स्वच्छ पेयजल से वंचित है। 6.3 करोड़ ग्रामीणों को साफ पानी नसीब ही नहीं है। देश के तीन चौथाई घरों में पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है।
देश में जलस्तर का लगातार गिरना, पानी की गुणवत्ता खराब होना और पानी के लिए पाइप लाइन न होने जैसी देशव्यापी समस्याएं व्यापक हैं। इस दिशा में 1980 के दशक में पर्यावरणविद जयंत बंधोपाध्याय ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा था कि- “जल की उपलब्धता और गुणवत्ता केन्द्रीय विषय रहेगी और भारत का भविष्य जल है, तेल नहीं।” तब उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन आज हर संवेदनशील व्यक्ति इस विषय की गंभीरता को जान-समझ चुका है। दरअसल यह संकट केवल पानी की कमी तक सीमित न होकर सभी क्षेत्रों यथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम जलस्रोतों पर भी दिखाई दे रहा है।
गौरतलब है कि धरती पर 97 फीसदी जल समुद्र का खारा पानी है जबकि केवल तीन फीसदी ही मीठा पानी है। यही हरेक जीव को जीवन दान देता है। फिर जब हम धरती के आकार, उस पर जैविक विविधता वाले पेड़-पौधों से छेड़छाड़ करते हैं, उस दशा में बारिश, जल प्रबंधन, जल उपलब्धता आदि सभी पर उसका व्यापक असर पड़ता है।
यह प्रकृति एक संसाधन के रूप में, स्रोत के रूप में, मित्र के रूप में हमारी आने वाली पीढि़यों को उपलब्ध रहे तो इसके लिए हमें अपनी संतति और आने वाली पीढि़यों के लिए अपनी जिम्मेदारी का अहसास करते हुए प्रकृति से मेलजोल और प्यार करना सीखना होगा।
पर्यावरण संरक्षण की आशा तभी की जा सकती है जब इसके लिए प्रशासन के साथ-साथ समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आये। देश की सुप्रीम अदालत भी मानती है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बेहद जरुरी है। देश की प्रगति तभी संभव है जबकि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रमुखता दी जाये। इस पर आगे विचार करने के लिए पर्यावरण समूह को आगे आना पड़ेगा तभी कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।
*वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद।