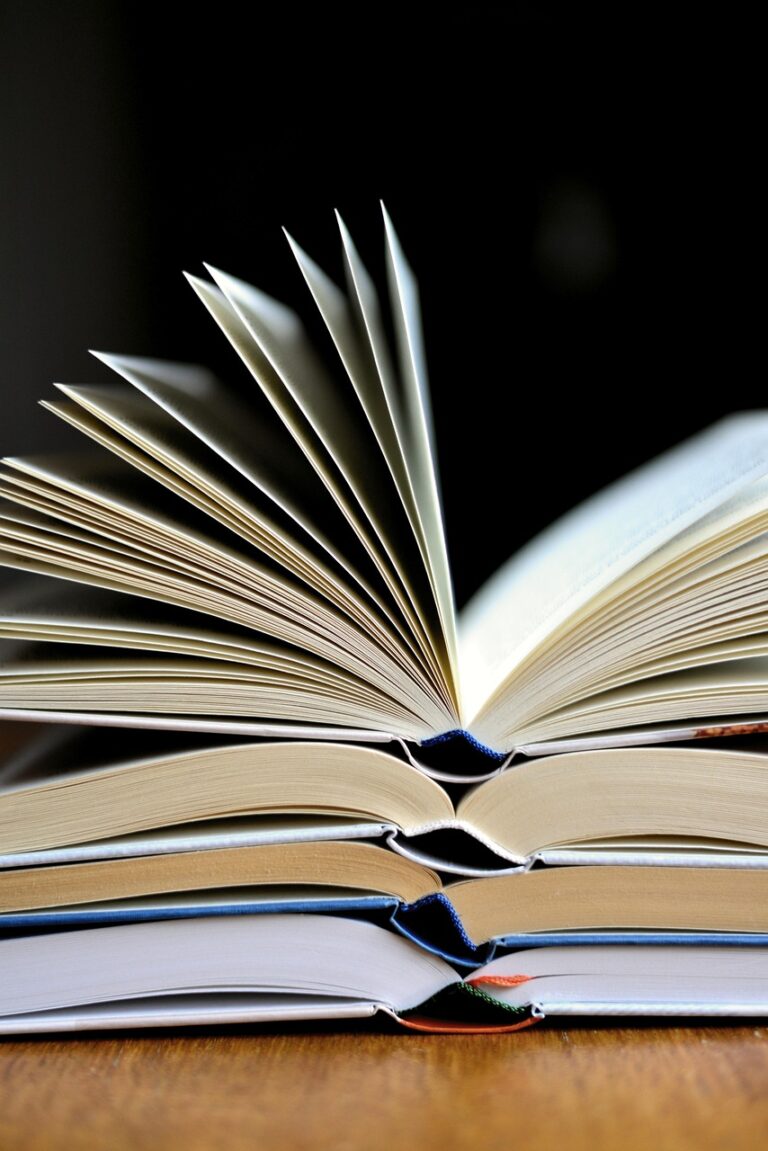ललितपुर/झांसी: बुंदेलखंड की धूल भरी गलियों में बसे सहरिया आदिवासी आज भी शिक्षा की रोशनी से कोसों दूर हैं। गरीबी और पलायन ने उनके बच्चों को स्कूल की बजाय मजदूरी की राह दिखाई। परन्तु झांसी के सिमिरिया गाँव में, एक बरगद की छाँव तले, बच्चे हँसते-खेलते अक्षरों से दोस्ती कर रहे हैं। यह छोटा-सा स्कूल उम्मीद की लकीर खींच रहा है, जो इन के भविष्य को नया रंग दे सकता है।
सहरिया समुदाय भारत के सबसे पिछड़े आदिवासी समुदायों में से एक है। झांसी और ललितपुर जिलों में इनके हजारों परिवार रहते हैं, परन्तु शिक्षा को लेकर जागरूकता की भारी कमी है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, इनकी साक्षरता दर मात्र 4.72% है, और महिलाओं में तो 2% से भी कम। यह भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाले समुदायों में से एक है। ललितपुर में सहरिया अनुसूचित जनजाति हैं, परन्तु झांसी में अनुसूचित जाति। ललितपुर में इनकी संख्या करीब एक लाख है, और झांसी में भी लगभग इतनी ही।
सहरिया समुदाय के लोग मुख्य रूप से दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं। जंगलों से लकड़ी और औषधीय जड़ी-बूटियाँ इकट्ठा करना, खेतों में मजदूरी करना और ईंट-भट्टों पर काम करना इनकी आजीविका के प्रमुख साधन हैं। अस्थायी और कम आमदनी वाले रोजगार के कारण ये परिवार एक स्थान पर टिककर नहीं रह पाते, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा आती है। बच्चे स्कूल में नामांकन तो करा लेते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्हें परिवार के साथ पलायन करना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई रुक जाती है। कई बच्चे कभी वापस स्कूल नहीं लौटते।
इसलिए शिक्षा से दूरी का एक और कारण समुदाय की सोच है। अधिकांश सहरिया परिवारों को लगता है कि पढ़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि रोजगार के अवसर फिर भी सीमित रहेंगे। उनका मानना है कि स्कूल भेजने से बेहतर है कि बच्चे कम उम्र से ही काम करना सीखें और परिवार की आर्थिक मदद करें। इस सोच के कारण माता-पिता खुद बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा को लेकर यह उदासीनता और अधिक देखने को मिलती है। कम संसाधनों के कारण प्राथमिक शिक्षा के बाद लड़कियों को स्कूल भेजना मुश्किल हो जाता है।
हालाँकि, सरकारी स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनका असर बहुत सीमित रहा है। गाँवों में बने सरकारी स्कूलों की स्थिति भी चिंताजनक है। कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, और जहाँ शिक्षक उपलब्ध हैं, वहाँ जातीय भेदभाव की वजह से आदिवासी बच्चों के साथ उपेक्षा की जाती है। कई जगहों पर स्कूलों में बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं हैं, जिससे बच्चों का वहाँ रुकना मुश्किल हो जाता है।

फिर भी, कुछ सकारात्मक बदलाव उभर रहे हैं। सिमिरिया गाँव में, जो झांसी से 19 किमी और लखनऊ से 349 किमी दूर है, एक अनौपचारिक स्कूल चल रहा है। यहाँ 36 सहरिया परिवारों के 200 लोग रहते हैं, जो दैनिक मजदूरी से गुजारा करते हैं। इस स्कूल में शिक्षिका मनीषा प्रजापति कहती हैं, “हमारे पास एक कमरा तो है, लेकिन मौसम के अनुसार हम बच्चों को बाहर पढ़ाना पसंद करते हैं।” बरगद की छाँव में बच्चे खेल और कला के जरिए गणित और भाषा सीखते हैं। उनकी रुचि बनी रहती है, और वे नियमित स्कूल आने लगे हैं। हाल ही में छह लड़कियों का कस्तूरबा गांधी विद्यालय में चयन हुआ, जो बड़ी उपलब्धि है।
मथुरापुर गाँव में, बबीना ब्लॉक के तहत, परमार्थ संगठन का एक स्कूल 25 बच्चों को पढ़ाता है। शिक्षिका रिंकी बिरथरे कहती हैं, “सबसे बड़ी समस्या बच्चों के पलायन के कारण पढ़ाई में व्यवधान आना है।” परन्तु वे बच्चों को संशोधन कार्य देती हैं, ताकि पढ़ाई न रुके। एक लड़की ने बताया कि उसने पलायन के दौरान किताबें और कॉपियाँ साथ रखीं और रास्ते में भी पढ़ाई की। यह हौसला सहरिया बच्चों की जिद दिखाता है।
गैर-सरकारी संगठन माता-पिता को समझा रहे हैं कि शिक्षा भविष्य बदल सकती है। कुछ सहरिया औरतें अब बेटियों को स्कूल भेजने लगी हैं। परन्तु लड़कियों के लिए रास्ता आसान नहीं। आठवीं के बाद सामाजिक रूढ़ियाँ और दूर के स्कूल पढ़ाई रोक देते हैं। परिवार जल्दी शादी को तरजीह देते हैं।
इसलिए समाधान जरूरी हैं। चलते-फिरते स्कूल पलायन में पढ़ाई जोड़ सकते हैं। आर्थिक मदद माता-पिता को स्कूल की ओर मोड़ेगी। गाँव के शिक्षक बच्चों को अपनी बोली में सिखाएँगे। सहरिया बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार, संगठन, और समुदाय को साथ चलना होगा। सिमिरिया और मथुरापुर की छोटी जीतें बता रही हैं कि बदलाव मुमकिन है।