
रविवारीय: नंबरों का खेल और खोता बचपन
अभी हाल ही में दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आए हैं। हर साल की तरह इस बार भी परिणाम के दिन एक अलग ही हलचल थी, एक उत्सुकता थी—घरों में बेचैनी, बच्चों की धड़कनों की रफ्तार और अभिभावकों की उम्मीदें… सब कुछ अपने चरम सीमा पर।
इस माहौल में अचानक मेरा मन थोड़ा पीछे चला गया—हम थोड़ी देर के लिए पुरानी यादों में खो गए। अपने समय की ओर। हमें अपना समय याद आ गया।
मुझे आज भी याद है वो सुबह, जब हमारा बोर्ड का रिजल्ट अखबार में आया था। हम सब नींद में ही थे। उनिंदी आंखों से अख़बार के पन्नों में अपना नाम और क्रमांक खोजने लगे। उस वक़्त नंबर नहीं छपा करते थे, सिर्फ श्रेणी बताई जाती थी—प्रथम, द्वितीय या तृतीय। स्कूल से नंबर मिला करते थे। मगर ‘प्रथम श्रेणी’ पास होना ही एक सामाजिक सम्मान था। कोई विशेष तैयारी नहीं, कोई कोचिंग नहीं, बस पाठ्यपुस्तकों से जितना समझ में आया, उसी को लिखकर परीक्षा दे दी जाती थी। हां, कभी कभी स्कूल के शिक्षकों से ट्यूशन ज़रूर लिया करते थे।
आज के दौर में बच्चे इस ‘नंबर गेम’ में कुछ इस तरह उलझ गए हैं कि लगता है जैसे संतोष नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं। किसी को 95% मिला है तो वो सोचता है कि 98% क्यों नहीं आया, और जिसे 98% आया है, वो 100% से चूक जाने का मलाल लिए बैठा है। अचरज तो तब होता है जब हिन्दी, अंग्रेज़ी, इतिहास जैसे विषयों में भी पूरे के पूरे नंबर मिलने लगे हैं। क्या वाकई इन विषयों में पूर्णता संभव है ? बच्चे तो ख़ैर बच्चे ही हैं। इस चूहा दौड़ में अभिभावक भी अपने आप को कहां पीछे छोड़ रहे हैं।
इस होड़ में बच्चों का बचपन कहीं खो गया है। खेल के मैदान खाली हैं, गलियों की चहल-पहल और चहक अब मोबाइल की स्क्रीन में कैद हो गई है। सामाजिक संवाद सिमट कर बस कोचिंग सेंटरों और टेस्ट सीरीज़ तक रह गया है। दबाव इतना अधिक है कि कई बार बच्चे इस बोझ को सहन नहीं कर पाते। उनकी आंखों में सपने कम और तनाव ज़्यादा दिखने लगा है।
कभी एक पल रुककर सोचिए—आपको क्या चाहिए ? नंबरों की मशीन बने बच्चे ? या फिर सोचने-समझने वाले, संवेदनशील इंसान ? अगर जवाब दूसरा है, तो उन्हें खुला आकाश दीजिए। उनकी रुचियों को पंख दीजिए, उनके अपने निर्णयों में उनका साथ दीजिए। हो सकता है उनका रास्ता आपके बनाए हुए नक्शे से अलग हो, लेकिन यकीन मानिए, वे अपनी मंज़िल खुद तय करेंगे—और वहां तक पहुंच भी जाएंगे।
हमें एक अदद नौकरी के लिए नहीं, वरन् संपूर्ण जीवन के लिए बच्चों को तैयार करना है। उन्हें सिर्फ अच्छे अंक नहीं, अच्छे मूल्य भी देने हैं। तब जाकर वे एक बेहतर इंसान, एक ज़िम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। और तब, शायद, हमारे चेहरे पर भी वो मुस्कान लौटेगी, जो कभी बचपन में बिना किसी नंबर के भी हुआ करती थी।






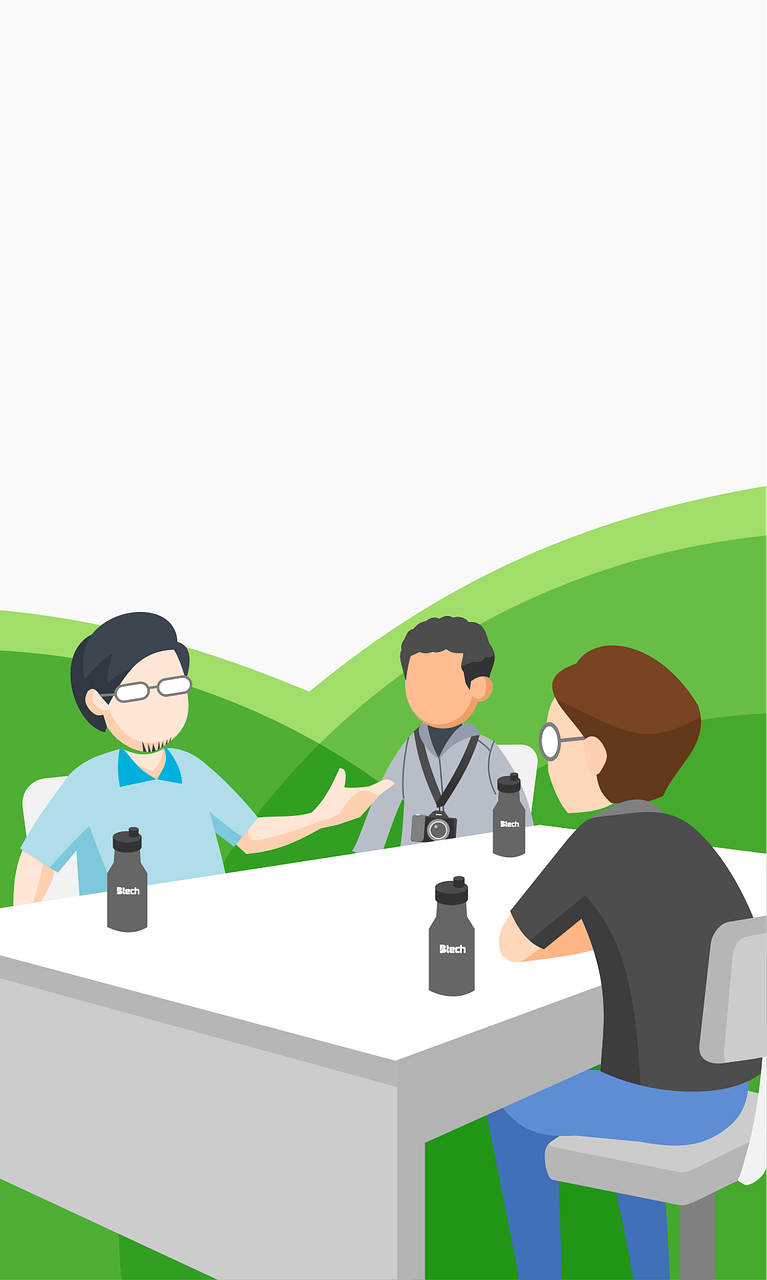
बिल्कुल सही…..गजल गायक पंकज उद्दाश के वो बोल एक ये भी है जमाना ,इक वो भी था जमाना
“नंबरों का खेल… और खोता बचपन”
यह ब्लॉग वर्तमान शिक्षा पद्धति की वास्तविकता को बेहद संवेदनशील और आत्ममंथन कराने वाले अंदाज में प्रस्तुत करता है। ब्लॉगर श्री वर्मा जी ने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि कैसे पहले पढ़ाई का उद्देश्य ज्ञान और समझ हुआ करता था, जबकि आज यह सिर्फ अंकों की होड़ बनकर रह गया है। बच्चों के बचपन पर पढ़ाई का भारी दबाव, कोचिंग संस्कृति और समाज की अपेक्षाएं उन्हें मानसिक तनाव की ओर धकेल रही हैं। यह ब्लॉग एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है—क्या हम बच्चों को नंबरों की मशीन बना रहे हैं या भावनात्मक रूप से मजबूत और सोचने वाले इंसान?
यह ब्लॉग एक सार्थक संदेश भी देता है कि बच्चों को नंबर नहीं-अवसर चाहिए, मार्ग नहीं- समर्थन चाहिए। यह विचार शिक्षा, अभिभावकत्व और समाज के लिए गहरी सोच की प्रेरणा है।